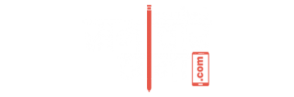जानें क्या है 'द ग्रेट गेम'? India Pakistan Tension के बीच Afghanistan ने कैसे दिया भारत का साथ?

7 से 10 मई 2025 तक के ये चार दिन भारत-पाकिस्तान के समकालीन इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। यह आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर भारत की एक बड़ी सैन्य, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। मात्र 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान का कोई भी कोना भारत के हमले से नहीं बचा। पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी है जिसे उसे समझाया नहीं जा रहा है और वह इसे पचा नहीं पा रहा है। इसलिए, पाकिस्तान के पास दुष्प्रचार युद्ध छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत के सटीक हमलों के बाद भी पाकिस्तान ने एक बार यह फैलाने की कोशिश की थी कि भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागी है।
अफगानिस्तान बना ढाल, पाकिस्तान की विश्वासघाती चाल
झूठ के पैर नहीं होते और सच हमेशा सतह पर आ जाता है। कमज़ोर और पाखंडी लोगों का सबसे बड़ा हथियार झूठ है। पाकिस्तान का धोखा उस समय उजागर हो गया जब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज्मी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने अफ़गानिस्तान पर कोई मिसाइल नहीं दागी है। इस झूठ को बुनने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान किसी तरह अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को इस युद्ध में घसीटना चाहता था? क्या उन्होंने हमेशा की तरह अफगानिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार को भारत के विरुद्ध करने का असफल प्रयास किया? यदि हां तो क्यों? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को फिर से उस महाखेल में घसीटना चाहता है जिसने अफगानिस्तान के इतिहास, राजनीति और समाज पर इतने गहरे दाग छोड़े हैं कि वह आज तक उनसे उबर नहीं पाया है।
दुनिया की बड़ी ताकतें अफगानिस्तान पर नजर गड़ाए हुए हैं
15 अगस्त, 2021 से अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार युद्धग्रस्त देश पर कब्जा कर रही है। तालिबान की नीतियाँ काफी कट्टरपंथी हैं। लेकिन तालिबान भी एक देश के शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। उन्हें यह समझ आ गया है कि अफगानिस्तान का असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जो इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हैं। लेकिन तालिबान यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन शक्तियों के चंगुल से कैसे निकला जाए और अफगानिस्तान को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए। 20 साल की उथल-पुथल के बाद चार साल पहले 2021 में दूसरी बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया तालिबान चाहता है कि दुनिया के देश उसकी सरकार को मान्यता दें। लेकिन उनकी कट्टरपंथी इस्लामी नीतियां, महिलाओं के अधिकारों पर उनका रुख अभी भी दुनिया को यह समझाने में असमर्थ हैं कि उन्हें मान्यता दी जाए या नहीं। लेकिन तालिबान अफगानिस्तान के विकास को लेकर गंभीर है और वह कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे अफगानिस्तान फिर से अस्थिरता की ओर धकेला जाए। इस मामले में भारत हमेशा से अफगानिस्तान का विश्वसनीय मित्र रहा है और वह हमेशा से पाकिस्तान के लिए बाधा बनता रहा है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान की पुरानी सरकारों की तरह तालिबान भी भारत से दोस्ती की अहमियत समझ रहा है।
भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश
भारत-पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। भारत ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान सरकार के रुख का स्वागत किया जिसमें तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के प्रयासों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज शाम अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। झूठी और निराधार रिपोर्टों के आधार पर भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनकी कड़ी अस्वीकृति का स्वागत करते हैं। पारंपरिक मैत्री और विकास आवश्यकताओं पर अफगान लोगों के साथ सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया तथा इस सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई।
2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान के साथ यह भारत की सबसे उच्च स्तरीय वार्ता थी। विदेश मंत्री स्तर की इस बातचीत से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसी साल जनवरी में दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें बनी समझ ही इस बैठक का आधार बनी...भारत ने भले ही अभी तालिबान सरकार को मान्यता न दी हो, उसके साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह बहाल न किए हों, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को कायम रखते हुए वह वहां के लोगों की खातिर बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगातार मदद करता रहा है...और तालिबान भी भारत के इस रुख का समर्थन करता रहा है और पारंपरिक दोस्ती को समझता है।
भारत में आतंकवादी हमले की निंदा और कूटनीतिक संदेश
विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के बाद तालिबान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने, व्यापार सहयोग और कूटनीतिक वार्ता पर चर्चा की। भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बताते हुए मुत्तकी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। उन्होंने दोहराया कि अफगानिस्तान सभी देशों के साथ संतुलित और रचनात्मक विदेश नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुत्तकी ने भारतीय वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने और भारतीय जेलों में बंद अफगान नागरिकों की रिहाई की मांग भी उठाई। तालिबान के अनुसार, जयशंकर ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की सराहना की और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने अफगान कैदियों और वीज़ा से संबंधित मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
चाबहार बंदरगाह और अफगानिस्तान-भारत सहयोग
तालिबान द्वारा जारी एक बयान में कहा गया इस बात पर गौर किया गया कि दोनों पक्षों ने ईरान में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास पर जोर दिया। इस बंदरगाह पर एक टर्मिनल का संचालन एक भारतीय कंपनी द्वारा किया जाता है और यह अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल रहा है। तालिबान ने चाबहार के रास्ते भारत से माल भेजने में रुचि दिखाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अफगानिस्तान को जमीनी रास्ते से आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है, जिससे चाबहार बंदरगाह की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं, पहलगाम हमले के बाद भी अफगानिस्तान का भारत के प्रति रवैया सहयोगात्मक और संतुलित रहा है।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यह इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान भारत के समक्ष मौजूद आतंकवाद की चुनौती को अच्छी तरह समझता है। इसके बावजूद पाकिस्तान और उसका रणनीतिक साझेदार चीन लगातार तालिबान को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है।
त्रिपक्षीय वार्ता और चीन-पाकिस्तान की भूमिका
जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अपने चरम पर था, तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का नवीनतम दौर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आयोजित किया गया था। 2017 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आपसी राजनीतिक विश्वास बढ़ाना, आतंकवाद के खिलाफ समन्वय स्थापित करना और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। चीन और पाकिस्तान उन कुछ देशों में शामिल हैं जिन्होंने तालिबान सरकार के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है, हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के तहत 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (सीपीईसी) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने तथा वहां निवेश बढ़ाने का इरादा रखता है। लेकिन इस राह में कई चुनौतियां हैं। तालिबान भी इस निवेश के महत्व को समझता है, लेकिन उन्हें यह भी आशंका है कि चीन इसके लिए ऊंची कीमत वसूलना चाहेगा।
डूरंड रेखा विवाद और टीटीपी का मुद्दा
तालिबान सरकार ब्रिटिश काल की डूरंड रेखा को पाकिस्तान की सीमा मानने से इनकार करती है। इसके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराना सीमा विवाद भी बना हुआ है। अफगानिस्तान का मानना है कि डूरंड रेखा उसकी क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है, विशेषकर पश्तून बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में। यही कारण है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में लगातार असंतोष बना हुआ है। यहां पश्तून संगठन नियमित रूप से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। इसके साथ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) भी पाकिस्तानी सेना और उसके ठिकानों पर हमले करता रहता है, जो पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को तालिबान सरकार का समर्थन प्राप्त है और यह दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण है।
हवाई हमले और बढ़ता सीमा तनाव
इन तनावों के बीच, पिछले दो वर्षों में तीसरी बार, दिसंबर 2024 में, पाकिस्तान ने अफगान धरती पर टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। ये हमले अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में हुए, जिनमें कई लोग मारे गए। तालिबान सरकार ने इन हमलों को बहुत गंभीरता से लिया और इसके बाद डूरंड रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। टीटीपी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमले तेज कर दिए तथा पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के कई कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। यह तनाव अभी भी बना हुआ है।
अफ़गान शरणार्थी और पाकिस्तान के साथ तनाव
अफगानिस्तान दशकों से गृहयुद्ध और जनजातीय संघर्षों से त्रस्त है, जिसके कारण वहां की एक बड़ी आबादी ने पाकिस्तान में शरण ली है। वर्तमान में पाकिस्तान में लगभग 35 लाख अफगान शरणार्थी रह रहे हैं, जो बहुत खराब मानवीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इनमें से कई शरणार्थियों को जबरन वापस भेज रहा है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस मानवीय राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है और आज उनके आपसी संबंध इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।
ऐतिहासिक दृष्टि से, अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए यह प्रतिस्पर्धा वास्तव में दोनों साम्राज्यों की रणनीति का हिस्सा थी, जिसके माध्यम से वे एक-दूसरे के विस्तार को रोकना चाहते थे। यह संघर्ष केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कूटनीति, जासूसी और स्थानीय कबीले नेताओं के साथ गठबंधन की जटिल राजनीति भी शामिल थी। अफ़गानिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया, जहां प्रत्येक पक्ष अपने प्रभाव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। ब्रिटेन और रूस के बीच संघर्ष केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं था। इसका प्रभाव मध्य और दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में देखा गया। मध्य एशिया की भूमि साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच शतरंज की बिसात की तरह बन गई, जिसके कारण कई युद्ध हुए। अफगानिस्तान का सामरिक महत्व इतना अधिक था कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यों के बीच इस पर प्रभाव के लिए संघर्ष हुआ। इस भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को "द ग्रेट गेम" कहा जाता है। यह शब्द प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग के उपन्यास किम से लोकप्रिय हुआ।
सोवियत सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए कई शक्तियां एक साथ आईं। परिणामस्वरूप, एक शांतिपूर्ण और सुंदर देश हिंसा, रक्तपात और युद्ध का क्षेत्र बन गया। दस वर्षों की लड़ाई के बाद अंततः सोवियत संघ को 1989 में अफगानिस्तान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
1979 के बाद से सबसे बढ़िया खेल
अफ़गानिस्तान को लेकर शुरू हुआ "ग्रेट गेम" अस्सी के दशक के अंत में और तेज़ हो गया, जब सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। यह घटना अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए एक बड़ा झटका थी। इन देशों ने सोवियत प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद, अफगानिस्तान विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। जो देश कभी उदार और प्रगतिशील रास्ते पर था, वह धीरे-धीरे कट्टरपंथी ताकतों के चंगुल में आ गया और अंतर-कबीले संघर्षों में उलझ गया। इन परिस्थितियों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान था, जिसने वहां लगातार अस्थिरता को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान को न तो अफगान लोगों के कल्याण की चिंता है, न ही उनके दीर्घकालिक हितों की।
इसके विपरीत, पाकिस्तान एक ओर पश्चिमी शक्तियों के पीछे खड़ा रहा और दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों को पोषित करता रहा। उन्होंने कभी भी अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की परवाह नहीं की। इसने कट्टरपंथी ताकतों को हर संभव सहायता दी - और आज अफगानिस्तान की स्थिति उसी का परिणाम है। इस सबके बीच, जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापस चली गईं, तो तालिबान ने बहुत जल्दी बलपूर्वक सत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया। पिछली तालिबान सरकार 1996 से 2001 तक चली, जिसे अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य अभियान द्वारा गिरा दिया गया था। वह सरकार केवल पांच वर्ष ही चल सकी। अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ बातचीत और संबंध सुधारने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। अब यह तालिबान पर निर्भर है कि वह किन लोगों पर शासन कर रहा है। वह अपनी कठोर नीतियों को नरम करने के लिए कितने इच्छुक हैं? भारत का उद्देश्य स्पष्ट है: जहां भी अफगान लोगों के हित में कोई संभावना है, भारत उसे वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
वास्तव में, यह अफगानिस्तान की वह तस्वीर है जो उसके इतिहास के स्वर्णिम युग की गवाही देती है। 1963 और 1973 के बीच का काल "स्वर्ण युग" के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब अफ़गानिस्तान एक उदार और आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहा था। वहां रहने, खाने, पहनने और काम करने की आजादी इतनी सहज थी कि कई यूरोपीय देशों की नीतियां भी पिछड़ी हुई लगती थीं। कई लोग शायद इस बात पर यकीन न करें, लेकिन अफगान महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में ही मिला। इसकी तुलना अमेरिका की महिलाओं से करें, जिन्हें यह अधिकार 1920 में और यूनाइटेड किंगडम की महिलाओं को 1918 में मिला - यानी, लोकतांत्रिक अधिकारों के मामले में अफगान महिलाएं दुनिया से पीछे नहीं, बल्कि आगे थीं।
1950 के दशक तक अफगानिस्तान में घूंघट प्रथा लगभग समाप्त हो गयी थी। महिलाएं शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं हाँ। 1964 में देश ने एक नया संविधान अपनाया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान अफगानिस्तान धीरे-धीरे आधुनिकता और प्रगतिशील सोच की ओर बढ़ रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर सत्तर के दशक के अंत तक का यह काल अफगानिस्तान के इतिहास में सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण काल माना जाता है। लेकिन इसके बाद देश को ऐसी दुर्दशा झेलनी पड़ी कि वह आज तक उबर नहीं पाया है। विदेशी हस्तक्षेप, गृहयुद्ध और कट्टरपंथ ने अफगान महिलाओं पर सबसे बुरा असर डाला है - जो महिलाएं कभी समाज के हर पहलू में सबसे आगे थीं, अब उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है।
आज की पीढ़ी जब उस दौर की तस्वीरें देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि अफगानिस्तान कभी इतना खुला, आधुनिक और प्रगतिशील देश था। इसलिए इन तस्वीरों को संरक्षित करना और उनकी सच्चाई जानना बहुत महत्वपूर्ण है - ताकि हम समझ सकें कि अफगानिस्तान की असली पहचान क्या थी, और इसे किसने और कैसे बदला।