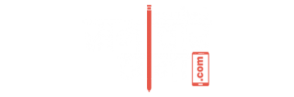वायरल डॉक्यूमेंट्री में देखे छप्पनिया अकाल को वो भयानक त्रासदी, जब भूख-प्यास से तड़पते लोगों की हालत देख राजस्थान की रेत भी रो पड़ी

राजस्थान के इतिहास में कई बार प्रकृति ने अपनी भयावहता दिखाई है, लेकिन साल 1899-1900 (संवत 1956) में पड़ा अकाल – जिसे 'छप्पनिया अकाल' कहा जाता है – वह सबसे भयावह त्रासदी बनकर उभरा। यह वह समय था जब न केवल खेत सूख गए थे, बल्कि लोगों की आंखों से भी आंसू सूख गए थे। पशु मरने लगे, इंसान एक-एक दाने को मोहताज हो गए, और चारों ओर फैली थी सिर्फ भूख, बदहाली और मौत की चुप्पी।
वर्ष 1899: जब मानसून ने साथ छोड़ दिया
छप्पनिया अकाल का नाम 'संवत 1956' के कारण पड़ा, जिसे हिंदी में "छप्पनिया" कहा गया। यह साल खेती-किसानी पर निर्भर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के लिए ऐसा साबित हुआ जिसे याद करना भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उस साल मानसून पूरी तरह नाकाम रहा। न खेतों में हल चले, न कुएं भरे। मवेशियों के चारे के लिए कुछ नहीं बचा। तालाब, बावड़ियां और नदी-नाले सब सूख गए।राजस्थान के अधिकांश हिस्सों – जैसे कि मारवाड़, मेवाड़, बांगड़, हाड़ौती और शेखावाटी – में हालात अत्यंत गंभीर हो गए थे। बीज बोने की आस तो दूर, खेतों की मिट्टी भी भुरभुरी होकर उड़ने लगी थी।
भुखमरी और पलायन
अकाल के कारण सबसे पहले पशुधन की तबाही शुरू हुई। चारे-पानी के अभाव में हजारों गायें, बैल, ऊँट और बकरी मरने लगे। पशु-आधारित कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद धीरे-धीरे भुखमरी का तांडव शुरू हुआ। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। कई लोग पेड़ों की छाल, घास, और सूखे पत्ते तक खाने को मजबूर हो गए।गांवों से हजारों की संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। लेकिन वहाँ भी हालात बेहतर नहीं थे। सरकार ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन संसाधनों की कमी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण मदद बहुत सीमित रही। लोग सड़कों पर मरने लगे। कई स्थानों पर लाशों को जलाने या दफनाने तक की व्यवस्था नहीं रह गई थी।
अकाल नहीं, मानो नरसंहार
इतिहासकारों और लोक कथाओं के अनुसार, इस भीषण अकाल में राजस्थान के लाखों लोग मारे गए। आंकड़ों के मुताबिक, अकेले जोधपुर रियासत में लगभग एक तिहाई जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि लोग अपने परिजनों को मरते हुए छोड़ने लगे थे।लोकगीतों और भजनों में आज भी उस समय का जिक्र सुनाई देता है –
"ना खेत बुवाई, ना घर में चूल्हा जल्यो, छप्पनिया रा दिन, हाड गळ्या पानी सूं"
(अर्थात: ना खेतों में फसल बोई गई, ना घर में चूल्हा जला, छप्पनिया के दिन ऐसे थे जब हाड़ पानी से गलने लगे।)
सामंती शोषण और सामाजिक ढांचा
छप्पनिया अकाल के दौरान केवल प्रकृति ही नहीं, बल्कि उस समय का सामंती शोषण भी आम जनता के लिए अभिशाप बन गया। जमींदारों और ठिकानेदारों ने राहत कार्यों के बदले लोगों से अत्यधिक श्रम लिया, लेकिन बदले में बहुत कम अनाज दिया। कहीं-कहीं तो "काम दो, खाना लो" की नीति भी अमानवीय रूप में सामने आई, जहां कमजोरों को बिना खाना दिए ही खदेड़ दिया गया।
समाज में स्थायी असर
छप्पनिया अकाल के सामाजिक प्रभाव बहुत गहरे थे। कई जातियों और वर्गों में स्थायी गरीबी उत्पन्न हुई। पारंपरिक ग्रामीण संरचनाएं टूट गईं। कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए और उनकी अगली पीढ़ियां भी गरीबी की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकीं।इस अकाल ने राजस्थान में लोकसाहित्य और गीतों के माध्यम से अपनी गहरी छाप छोड़ी। आज भी कई वृद्ध अपने बचपन में सुनी गई उन कहानियों को भावुक होकर सुनाते हैं, जिसमें छप्पनिया अकाल का उल्लेख होता है।
शासन की भूमिका और जागरूकता
ब्रिटिश शासन के तहत राहत कार्य तो शुरू हुए थे, लेकिन वे अपर्याप्त और असंवेदनशील थे। लोगों को काम के बदले भोजन देने की नीति अपनाई गई, मगर भारी श्रम और नाममात्र भोजन के चलते मौतें कम नहीं हुईं। कई विद्वानों का मानना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने समुचित जल प्रबंधन और राहत वितरण किया होता, तो इतने व्यापक पैमाने पर मौतें रोकी जा सकती थीं।