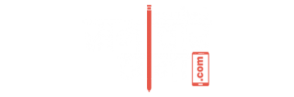हमारी पृथ्वी अनगिनत रहस्यों की साक्षी है। हर देश में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे दूसरे से अलग बनाती हैं। जैसे हमारे देश भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार या बुलंद दरवाजा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें साल में दो बार अपनी घड़ियों का समय बदलना पड़ता है। आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा लेकिन यह बिल्कुल सच है कि ये देश साल में दो बार अपनी घड़ियों का समय समायोजित करते हैं। क्योंकि इन देशों में घड़ी का समय हर साल लगभग एक घंटा आगे-पीछे हो जाता है। इस प्रणाली को डेलाइट सेविंग टाइम माना जाता है।
खैर, इस प्रणाली को समझना कोई पहेली नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में साल के 8 महीनों के लिए घड़ी एक घंटा आगे बढ़ जाती है और बाकी 4 महीनों के लिए एक घंटा पीछे चली जाती है। अमेरिका में मार्च के दूसरे रविवार को घड़ियाँ एक घंटा आगे और नवम्बर के पहले रविवार को एक घंटा पीछे कर दी जाती हैं। आइये जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है?
पुराने समय में यह माना जाता था कि इस प्रक्रिया से दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग होने के कारण किसानों को अतिरिक्त कार्य समय मिलता था। लेकिन, समय के साथ यह धारणा बदल गई है। अब यह प्रणाली बिजली की खपत कम करने के उद्देश्य से अपनाई गई है। अर्थात्, गर्मी के मौसम में घड़ी को एक घंटा पीछे करके, दिन के उजाले का अधिक उपयोग करने के लिए मानसिक रूप से एक घंटा अतिरिक्त मिल जाता है।
विश्व के लगभग 70 देश इस प्रणाली को अपनाते हैं। हालाँकि, भारत और अधिकांश मुस्लिम देशों में इस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है। अमेरिकी राज्य कानूनी तौर पर इस प्रणाली का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे इस प्रणाली को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यूरोपीय संघ में शामिल देश इस प्रणाली को अपनाते हैं।
इस प्रणाली को अपनाने के पीछे कारण ऊर्जा की खपत को कम करना था, लेकिन विभिन्न अध्ययनों में अलग-अलग आंकड़े दिए गए हैं। इसीलिए इस प्रणाली पर हमेशा बहस होती रहती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कहा था कि इस प्रणाली से लगभग 0.5 प्रतिशत बिजली की बचत हुई, लेकिन नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने उसी वर्ष एक अध्ययन में कहा कि इस प्रणाली के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हुई।
.
यह प्रणाली अमेरिका में वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। लेकिन डेलाइट सेविंग की प्रणाली काफी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में अपने एक पत्र में इसका पहली बार उल्लेख किया था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी जैसे कई देशों में इस प्रणाली को अपनाया गया था।